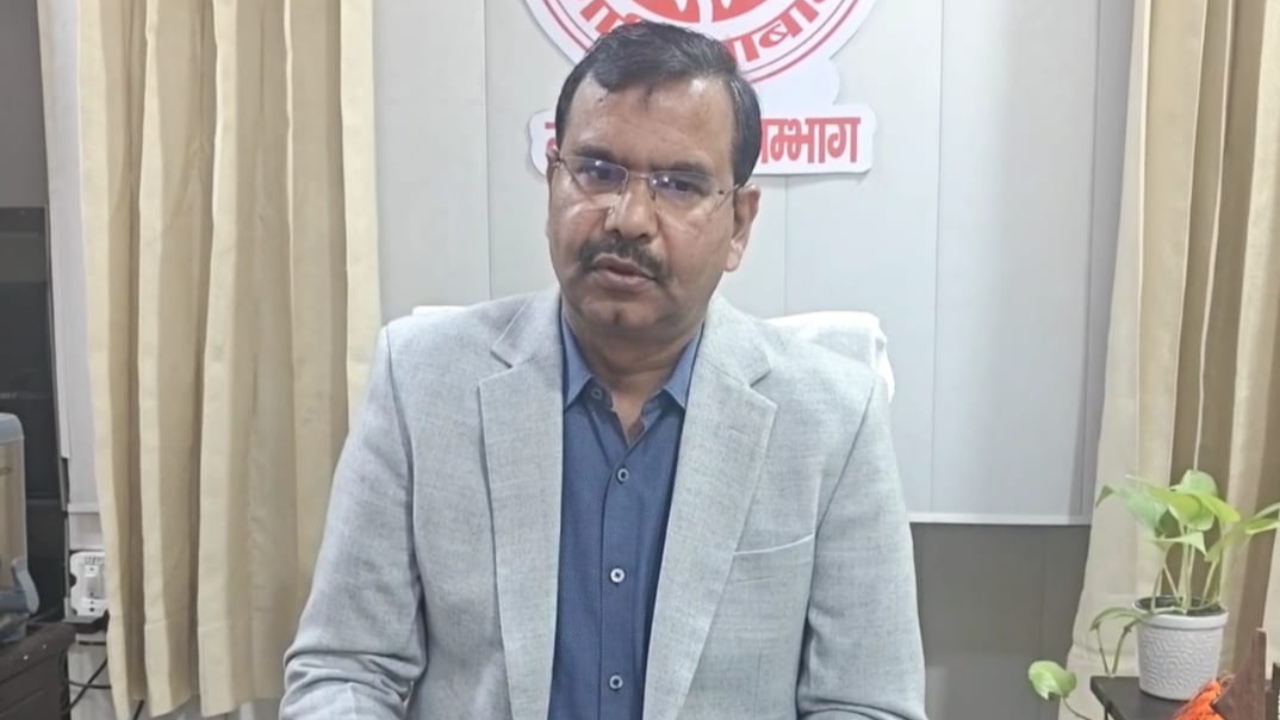शिक्षक का गैर-शैक्षिक कार्य का बोझ पढ़ाई की नींव को कर रहा कमजोर
देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लगातार नए-नए अवसर के लिए प्रयास लिए जा रहे है। एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), निपुण भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। शिक्षक, जिन्हें समाज का निर्माता और राष्ट्र का भविष्य गढ़ने वाला माना जाता है, आज शिक्षण से अधिक गैर-शैक्षणिक कार्यों में उलझे हुए हैं। यह न केवल एक पेशागत अन्याय है, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी की नींव को भी कमजोर कर रहा है। ग्रामीण भारत में जाकर जब प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति देखी जाती है, तो यह सच्चाई सामने आती है कि शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी स्कूल में एक ही शिक्षक पाँच कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विवश है, तो कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका हुआ मिलता है क्योंकि कार्यकर्ता मोबाइल फेस मैपिंग या अन्य सरकारी सर्वेक्षणों में व्यस्त है। चुनाव ड्यूटी, मतदाता सूची का सत्यापन, जनगणना, शौचालय की सफाई की निगरानी, मध्यान्ह भोजन योजना का प्रबंधन, छात्रवृत्ति का सत्यापन, यूनिफॉर्म वितरण, प्रशासनिक काम और लगातार रिपोर्टिंग—ये सारे काम शिक्षक के जिम्मे डाल दिए गए हैं। परिणाम यह होता है कि कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का समय और उत्साह दोनों कम हो जाते हैं।
शिक्षक की पहचान हमेशा ज्ञान देने वाले मार्गदर्शक और आदर्श के रूप में रही है। लेकिन आज वही शिक्षक प्रशासनिक बोझ तले दबकर “क्लर्क” या “फील्ड वर्कर” बन गया है। एक अंग्रेजी शिक्षक, जो बच्चों को भाषा और साहित्य में निपुण बनाने का सपना लेकर इस पेशे में आया था, आज फाइलों और आंकड़ों में उलझा हुआ है। वह दिन भर पर्चियाँ बांटने, आंकड़े भरने और सरकारी बैठकों में भाग लेने को मजबूर है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की असफलता का प्रतीक है। भारत में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन जब शिक्षक स्वयं ही बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते, तो इस कानून का पालन केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। पाँच कक्षाओं को एक शिक्षक द्वारा संभालना, या बच्चों को बिना शिक्षक के बैठा देना, बच्चों के सीखने के अधिकार का खुला उल्लंघन है। जब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत भयावह होता है। कक्षा में जब शिक्षक निरुत्साहित होकर केवल औपचारिकता निभाता है, तो बच्चे रचनात्मकता और तार्किकता विकसित नहीं कर पाते। वे डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वास्तविक ज्ञान, कौशल और समझ की गहराई से वंचित रहेंगे। ऐसी पीढ़ी देश की बौद्धिक संपदा और नवाचार क्षमता को कमजोर कर देगी। यदि हम विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था देखें, तो पाते हैं कि वहाँ शिक्षकों को केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाता है। प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग संवर्ग होता है। वहाँ शिक्षक का सम्मान केवल वेतन या पुरस्कारों से नहीं, बल्कि उसके कार्यक्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा से भी होता है। भारत में यदि हम “विश्वगुरु” बनने का सपना देख रहे हैं, तो हमें भी शिक्षकों को उसी प्रकार स्वतंत्र और सक्षम बनाना होगा।
शिक्षक और छात्र—दोनों पर मानसिक बोझ, शिक्षकों पर जबरदस्ती का काम डालने से उनकी मानसिक थकान बढ़ती है। वे शिक्षण को बोझ समझने लगते हैं और कक्षा में उनकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। दूसरी ओर, छात्र भी जब अपने शिक्षक को असमर्थ या उदास देखते हैं, तो उनका सीखने का उत्साह घट जाता है। यह स्थिति एक “नकारात्मक चक्र” पैदा करती है, जिसमें न शिक्षक प्रसन्न रह पाते हैं और न ही छात्र लाभान्वित हो पाते हैं। नीतिनिर्माता अक्सर तर्क देते हैं कि प्रौद्योगिकी ने काम को आसान बनाया है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो यह शिक्षकों पर और अधिक बोझ डाल रही है। मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना, डेटा अपलोड करना, अलग-अलग पोर्टलों पर रिपोर्ट डालना—ये सब शिक्षकों के लिए झंझट बन गए हैं। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सरलता लाना था, लेकिन यह शिक्षकों की स्वतंत्रता छीन रही है।
इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे— गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग संवर्ग : BLO, सर्वेक्षण, जनगणना, चुनाव जैसे कार्यों के लिए विशेष प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। प्रौद्योगिकी का स्मार्ट उपयोग : ऐसे डिजिटल टूल विकसित हों, जो शिक्षकों का समय बचाएं, न कि और अधिक लें। नीतिगत दृढ़ता : सरकारें यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक का प्राथमिक और एकमात्र काम शिक्षण ही रहे। शिक्षक प्रशिक्षण और प्रेरणा : शिक्षकों को लगातार अपडेटेड प्रशिक्षण मिले, जिससे वे नई शिक्षण पद्धतियों के साथ उत्साहपूर्वक काम कर सकें। जवाबदेही की स्पष्टता : शिक्षा विभाग को यह तय करना होगा कि उसकी पहली जवाबदेही बच्चों की शिक्षा है, न कि प्रशासनिक आंकड़ों का प्रबंधन। शिक्षक का स्थान ब्लैकबोर्ड के सामने है, न कि फाइलों और चुनावी पर्चियों के ढेर के बीच। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है, तब तक कोई भी नीति या अभियान सफल नहीं होगा। शिक्षकों को सम्मान और स्वतंत्रता दिए बिना, हम “विकसित भारत” और “विश्व गुरु” बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। आज ज़रूरत है कि हम अपने शिक्षकों को “क्लर्क” नहीं, बल्कि “नेशन बिल्डर” की भूमिका में वापस लाएँ। यही राष्ट्र और भविष्य, दोनों के हित में सबसे बड़ा निवेश होगा।
लेखक
श्याम कुमार कोलारे